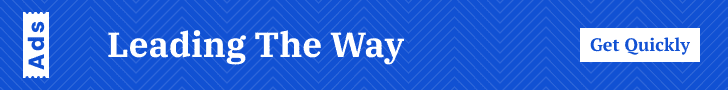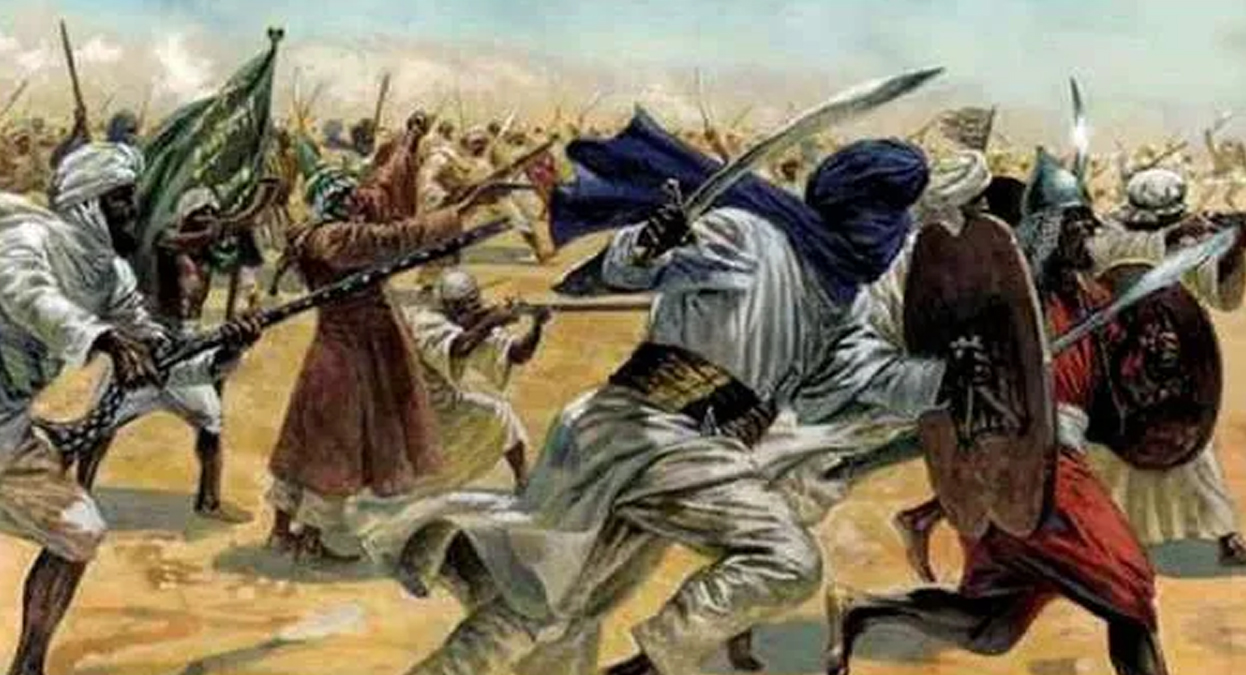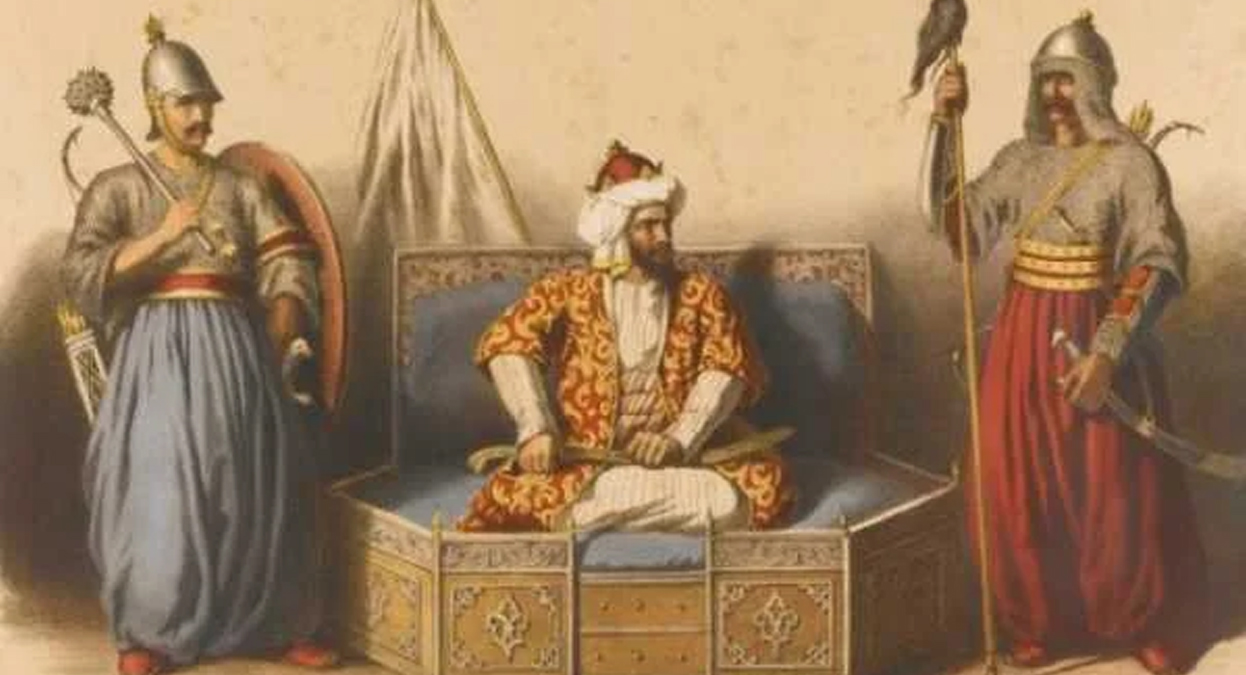
गुलाम वंश की शुरुआत सन 1206 में ‘मोहम्मद गौरी’ की मृत्यु के बाद हुई। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के सबसे विश्वास पात्र गुलामों में से एक हुआ करते थे। इसी कारण उनकी मृत्यु के बाद उनका सिंहासन ऐबक ने संभाला और यहीं से ‘गुलाम वंश’ की स्थापना शुरू हुई। ऐबक में एक महान शासक होने के सभी गुण विद्यमान थे। लेकिन उनका शासनकाल केवल 4 वर्ष तक ही रहा। 1210 ईस्वी मे घोड़े से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह अपने वंश की नींव मजबूत कर गए। ऐबक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ‘आरामशाह’ को सुल्तान बनाया गया और इस तरह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच इस वंश में कई शासकों ने भारत पर शासन किया।
इस वंश का नाम भी अपने आप में एक इतिहास है। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के ज्यादातर शासक “गुलाम” अर्थात “दास” हुआ करते थे। यहाँ तक कि इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक भी मुहम्मद गोरी के गुलाम थे। जिसके कारण ही इस वंश का नाम ‘गुलाम वंश’ पड़ा। हालांकि इस वंश को ‘मामलूक वंश’ या ‘दास वंश’ के नाम से भी जाना जाता था।
गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था, यह वंश भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था, जिसकी स्थापना ‘सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक’ ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क शासक थे, जिन्होंने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1210 तक शासन किया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 से 1210)
कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह केवल 4 वर्ष ही सुल्तान रहा। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। 1206 में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसका कारण था दरबार के अन्य गुलाम सरदारों का उससे ईर्ष्या करना।
अपनी मृत्यु के पूर्व मोहम्मद गोरी ने अपने उत्तराधिकारी के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा था। वह तुर्क दासों पर अधिक विश्वास करता था।मुहम्मद गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि प्रदान की लेकिन उसे सभी गुलाम सरदारों का प्रमुख बनाने का निश्चय नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विषम परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक काम किया और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक बना। गौरी के जीते हुए प्रदेशों का सूबेदार बनने से लेकर अपनी मृत्यु तक कुतुबुद्दीन ऐबक विद्रोह और युद्ध में ही व्यस्त रहा।
ऐबक ने गोरी के सहायक के रूप में कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लेकर अपनी योग्यता का परिचय दे दिया था। इसी बात से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। गोरी के चले जाने के बाद राजपूत कुछ शक्ति जुटाकर तुर्कों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन ऐबक ने 1192 ईस्वी में अजमेर तथा मेरठ में विद्रोह का दमन किया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। इससे पहले भारत पर किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभाव और शासन इतने ज्यादा समय तक नहीं टिका था।
उसने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर पुनः अधिकार किया। उसने 1194 में अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया और कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में मार डाला। 1197 ईस्वी में उसने भीमदेव की राजधानी अन्हिलवाड़ को लूटा और अत्यधिक धन प्राप्त किया। 1197 से 98 ईस्वी के बीच उसने चंदावर तथा बदायूं पर कब्जा जमा लिया। और साथ ही बनारस पर भी आक्रमण किया। उसने कालिंजर और महोबा पर आक्रमण करके महोबा के राहिल देव बर्मन द्वारा नौवीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को नष्ट कर दिया और खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया।
लेकिन इसी समय मोहम्मद गोरी के एक सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक पूरे समय विद्रोह को दबाने में व्यस्त रहा। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान अर्थात् पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई।
उन्होंने दिल्ली में ‘कुव्वत-उल-इस्लाम’ नामक मस्जिद, अजमेर में ‘अढ़ाई दिन का झोम्पड़ा’ नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने ‘सूफी संत ख्वाज़ा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी’ के सम्मान में दिल्ली में प्रसिद्ध ‘कुतुबमीनार’ का भी निर्माण करवाया था। ऐसे में उनकी कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार एवं सैनिक कुशलता के कारण उन्हें ‘लाख बख्श’ की उपाधि दी गयी।
इल्तुतमिश (1211 से 1236)
वास्तविक रुप से इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था क्योंकि उसे बगदाद के खलीफा से 1229 में सुल्तान पद का प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश एक वैध सुल्तान तथा दिल्ली सल्तनत, एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गई। खलीफा के इस स्वीकृति से सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने में सहायता मिली।
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। खोखरों के विरुद्ध उसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया था। अतः उसकी मृत्यु के बाद उसके अयोग्य पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। उसकी अयोग्यता के कारण दरबार के तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। फलस्वरुप इल्तुतमिश और आराम शाह में संघर्ष हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना।
सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जिसके पीछे का कारण था गद्दी के लिए अनेक दावेदारों का होना। गुलाम वंश के शासन काल में दरबार में षड्यंत्र आम बात थी। इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास ना करते हुए अपने विश्वस्त 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे ‘तुर्गान-ए-चिहलगानी’ नाम दिया। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है।
1215 से 1217 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल शत्रु एल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा से संघर्ष करना पड़ा। परिणामस्वरूप 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दौज को और 1217 ईस्वी में कुबाचा को पराजित कर दिया। अंत में सिंधु नदी में डूबने के कारण कुबाचा की मौत हो गई। इस तरह इल्तुतमिश के दोनों प्रबल विरोधियों का अंत हो गया।
इल्तुतमिश के समय में ही भारत पर मंगोल आक्रमण की संभावना बन रही थी। चंगेज खान अपने एक शत्रु जलालुद्दीन मुगबर्नी का पीछा करता हुआ 1221 ईस्वी में सिंध तक आ पहुंचा। कहा जाता है कि मुगबर्नी और चंगेज खां की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। चंगेज खान ने इल्तुतमिश से मुगबर्नी को शरण ना देने का आग्रह किया। परंतु 1228 ईस्वी में मुगबर्नी के भारत से वापस चले जाने पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया।
इल्तुतमिश भी ऐबक की तरह अपने शासनकाल में कई विद्रोह के दमन और विजय अभियानों में शामिल रहा। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक के विरुद्ध अभियान छेड़ा। और 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर तथा 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कर लिया। परंतु 1227 ईस्वी में मेवाड़ के जैत्र सिंह के विरुद्ध भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजय का सामना करना पड़ा। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के शासक मंगल देव को पराजित किया। 1235 में चंदेलों के विरुद्ध भी उसका अभियान सफल रहा, किंतु नागदा के गुहिलौतों और गुजरात के चालुक्यों के विरुद्ध इल्तुतमिश की हार हुई। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान अर्थात् अफगानिस्तान के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान वह बीमार पड़ गया और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।
इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। उसने सिक्कों पर “टकसाल” का नाम अंकित करवाने की परंपरा को प्रारंभ किया। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख “खलीफा” के प्रतिनिधि के रूप में किया। इल्तुतमिश ने “इक्ता” व्यवस्था का प्रचलन किया। अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया।
रजिया सुल्तान (1236 से 1240)
रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और उसे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। इल्तुतमिश के बड़े बेटे की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के कारण इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया को सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों का अभ्यास कराया गया था। 1231ईस्वी में अपने ग्वालियर अभियान के समय इल्तुतमिश ने दिल्ली के प्रशासन का कार्यभार रजिया को सौंपा था।
दिल्ली सल्तनत के सरदारों को इल्तुतमिश का किसी महिला को उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार नहीं था अतः उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के छोटे बेटे रुकनुद्दीन को सिंहासन पर बैठाया गया। जो रजिया सुल्तान का सौतेला भाई था। लेकिन यह अयोग्य और लापरवाह शासक निकला, जिसके 6 महीने के शासनकाल में उसकी माता शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान रजिया की हत्या करवाना चाहती थी। किंतु रजिया ने अयोग्य शासक के खिलाफ जनता के आक्रोश का फायदा उठाकर रुकनुद्दीन और उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या करवा दी। इसके बाद किसी अन्य उचित विकल्प के अभाव में रजिया को दिल्ली की गद्दी मिल गई।
सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के बाद रजिया सुल्तान ने पुरुषों का वेश धारण करना पसंद किया। वह दरबार में बिना परदे के आने लगी।वह अन्य पुरुष सम्राटों की तरह दिल्ली की गलियों में हाथी के ऊपर बिना नकाब के घूमने लगी। उसने महिला अंग रक्षकों की भी नियुक्ति की। रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका सिद्ध हुई।वह अपनी सेना तथा जनसाधारण का ध्यान अच्छे से रखती थी। उसने गैर तुर्कों को राजदरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। जिससे कुछ तुर्क अमीर नाराज हो गए।
रजिया के राज्याभिषेक के समय जो कुछ तुर्क अमीर उसका समर्थन कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि रजिया एक कठपुतली शासिका रहेगी। लेकिन जब रजिया ने शासन कार्यों में अपना आदेश चलाना शुरु कर दिया तब यह तुर्क सरदार उससे नाराज हो गए और उसके विरुद्ध षडयंत्र करने लगे। रजिया का याकूत जैसे गैर तुर्कों को उच्च पदों पर नियुक्त करना इन्हें सहन नहीं हुआ।
इसी बीच भटिंडा के राज्यपाल मलिक अल्तूनिया ने अन्य विद्रोही प्रांतीय राज्यपालों के साथ मिलकर रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रजिया ने याकूत के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जिसमें याकूत मारा गया।अपनी मृत्यु के भय से रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया। इधर दिल्ली में रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम ने शासन पर कब्जा कर लिया था। रजिया ने अल्तूनिया के साथ मिलकर पुनः दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन उसकी हार हुई। रजिया की सेना ने उसका साथ छोड़ दिया और उसे दिल्ली से भागना पड़ा।… माना जाता है कि कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा हरियाणा के कैथल में रजिया और अल्तूनिया की 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हत्या कर दी गई।
गैर विद्रोहियों के विरुद्ध रजिया का पहला सैनिक अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था। जहां के चाहमान शासक ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। रजिया ने रणथंभौर के विरुद्ध सेना भेजी लेकिन उसे इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उस समय चाहमानों ने मेवातियों के साथ मिलकर वर्तमान राजस्थान के अधिकांश उत्तर पूर्व के भागों पर कब्जा कर लिया था और दिल्ली के आसपास छापामार युद्ध करते रहते थे।
अन्य शासक
रज़िया बेगम की मौत के बाद इल्तुतमिश वंश के अन्य कई शासकों ने भारत पर शासन किया, लेकिन वह इतने कुशल नहीं थे इसलिए उनका शासन अधिक समय तक नहीं चल सका। रज़िया बेगम के बाद इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र बहरामशाह शासक बना, उसके बाद मसूदशाह शासक बना, वह रुकनुद्दीन का पुत्र था, मसूदशाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया गया।
गयासुद्दीन बलबन (1266 से 1287)
बलबन एक क्रूर शासक था जिसने निर्दयतापूर्वक अपने विद्रोहियों का दमन करवाया।जियाउद्दीन बरनी के अनुसार उसने सामान्य लोगों में शासक का भय स्थापित किया। उसने जनता से कहा कि सुल्तान धरती पर जिल्ले इलाही अर्थात् ईश्वर की छाया है। उसने अपने दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया।बलबन का दरबार सादगी से परिपूर्ण रहता था जहां कोई हंसी मजाक नहीं होती थी। उसने शराब और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने सुल्तान के सम्मान में ईरानी प्रथा “सिजदा एवं पैबोस” को प्रारंभ करवाया। बलबन ने ही फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज अर्थात् नववर्ष के त्यौहार को भी प्रारंभ करवाया था।
बलबन ने 40 सरदारों के समूह “चिहलगानी” को समाप्त कर दिया।बलबन आश्वस्त रहना चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति सुल्तान के प्रति वफादार रहे। इस कारण उसने योग्य जासूसी प्रणाली स्थापित की। वह अपने राज दरबारियों को छोटी गलती के लिए भी कड़ी सजा देता था। बलबन के समय ही पंजाब में बड़े पैमाने पर लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ।
मेवातियों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए उसने दिल्ली के बाहर स्थित जंगलों को कटवा दिया। नगर के सीमा पर सैनिक चौकियां स्थापित की और जंगल से होकर जाने वाले रास्तों को सुरक्षित बनाया। उसने कठोर “लौह एवं रक्त की नीति” का पालन किया। बलबन ने दरबारी अमीरों की जागीरें छीन ली एवं उनके बीच वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया।
बलबन इल्तुतमिश के 40 प्रमुख गुलाम सरदारों में से एक था। वह नसीरूद्दीन महमूद का वजीर भी था।मसूद शाह के पतन और नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने में बलबन की विशेष भूमिका थी। नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाकर वह स्वयं उसका वजीर बन गया। सुल्तान नासिरउद्दीन का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था अतः उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन 1266 ईस्वी में 60 साल की उम्र में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा।
उसने वजीर रहते हुए भी कई विजय अभियान चलाया। उसने दिल्लीवासियों को परेशान करने वाले मेवातियों का दमन किया और बंगाल पर पुनः कब्जा जमाया। उसने रणथंभौर के किले की घेराबंदी की लेकिन असफल रहा पर उसने राजपूतों से ग्वालियर छीन लिया। 1247 ईस्वी में उसने कालिंजर के चंदेल मुखिया के विद्रोह का दमन किया।
बलबन गुलाम वंश का पहला शासक था, जिसने मंगोलो का सफलतापूर्वक सामना किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मंगोल आक्रमण के भय को रोकने के लिए बलबन ने एक सुनिश्चित योजना बनाई। पश्चिमोत्तर सीमा पर उसने कई किले बनवाए और उनमें बड़ी संख्या में सैनिकों की नियुक्ति की। उसने मंगोलो के खतरों से दिल्ली सल्तनत को मुक्त किया लेकिन मंगोलो के आक्रमण का सामना करते हुए उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद खान की 9 मार्च 1285 को मौत हो गई थी। उसका दूसरा पुत्र बुगरा खान जो बंगाल का गवर्नर था उसने दिल्ली का सुल्तान बनने से इनकार कर दिया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा भी की लेकिन मंगोलों को रोकने के प्रयास में 1287 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गयी। और फिर,उसके पोते कैकाबाद को सुल्तान बनाया गया जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ।
गुलाम वंश का अंत
गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत काल में शासन करने वाला पहला वंश था जिसने 84 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। इस वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसके बाद कई उत्तराधिकारी आये और इस वंश का विस्तार किया लेकिन 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक समसुद्दीन क्यूमर्श की हत्या कर दी और इस तरह ‘गुलाम वंश’ समाप्त हो गया, और इसके स्थान पर ‘खिलजी वंश’ आया, जो दिल्ली सल्तनत का ‘दूसरा राजवंश’ बना।