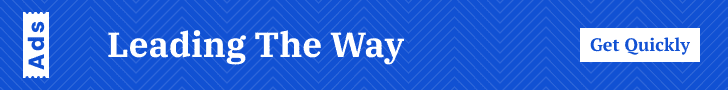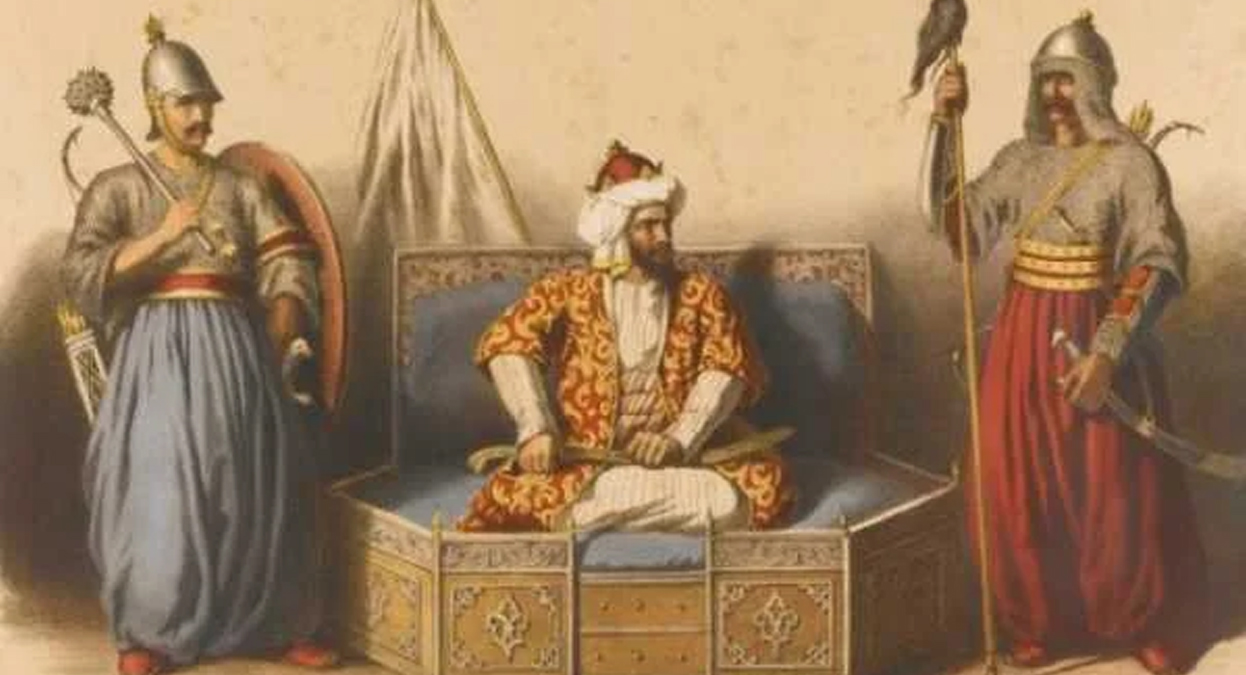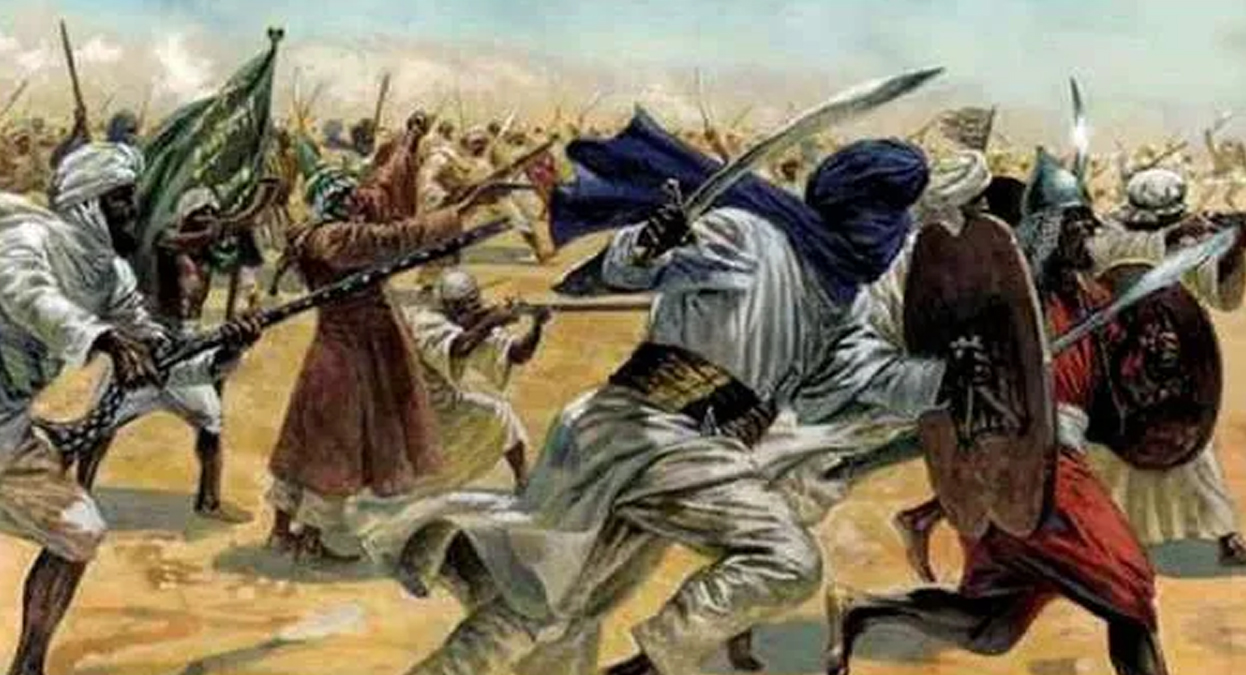समान नागरिक संहिता मतलब है, कि समाज के सभी वर्गों के साथ, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और संपत्ति का उत्तराधिकार जैसे मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। यह इस आधार पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में कानून और धर्म के बीच कोई संबंध बरकरार न रहे।
भारत “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र” है। विविधता भारत का सार है, लेकिन कानून में विविधता अन्यायपूर्ण है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि देश के कानून के मामले में हर व्यक्ति एक ही पायदान पर है, लेकिन कानून बनाने और उन्हें लागू करने के बीच हमेशा से एक अंतर रहा है। तीन तलाक पर हालिया फैसला उन मुद्दों का संकेत है जिनका सामना मुस्लिम महिलाएं प्राचीन काल से करती आ रही थीं और जो कदम उठाने की जरूरत थी, वह समय पर नहीं किए गए।
सवाल उठता है कि जब हर कोई देश के शासन के अधीन है तो अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग नियम क्यों बनाए गए हैं?
135 करोड़ विविधता को स्वीकार किया जाता है लेकिन इन सभी विविधताओं को एक ही नियम में क्यों नहीं बांध दिया जाता ताकि हर व्यक्ति सही मायने में एक हो जाए।
कानून का संरक्षण और मौलिक अधिकारों की स्थापना न केवल नागरिकों तक फैली हुई है, बल्कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी है। कोई भी भेदभाव, चाहे वह कुछ भी हो, हमारे कानून की सुरक्षा और कानून की समानता को परेशान करता है।
नमस्कार आप देख रहे है ज्ञानी रैबिट के बैनर तले “आज़ादी की ओर”,तो आइए हम चलते है, इस सीरीज के अगले एपिसोड की ओर,जँहा हम भारत के संदर्भ में “एक राष्ट्र एक कानून “से जुड़े इसके विविध आयामों पर चर्चा करेंगे।
भारत जैसे देश में जहां नागरिकों द्वारा विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है, समान नागरिक संहिता एक ऐसा बहस का विषय है जो वास्तव में सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या यह वास्तव में भारतीय व्यक्तिगत कानूनों के लिए एक बेंचमार्क होगा या नहीं।
समान नागरिक संहिता कानूनों का एक अलग समूह है जो मुख्य रूप से भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी भेदभाव या धर्म की परवाह किए बिना भारत के नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है।
इसका सीधा मतलब यह है कि कानूनों का एक अलग सेट भारतीय नागरिकों की अलग-अलग धर्म संस्कृति के सभी चल रहे कानूनों को प्रतिस्थापित करने जा रहा है।
भारत देश में समान नागरिक संहिता की मांग उस समय से चली आ रही है जब 20 वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने इसे महिलाओं के समान अधिकारों और सुरक्षा के साथ-साथ समानता और समानता के मुख्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया था। आजादी के दौरान महिलाओं की स्थिति और विशेषकर हिंदू विधवाओं के प्रति होने वाले गलत कार्यों को सुधारने के विचार को ध्यान में रखते हुए कई सुधार कानून पारित किए गए।
हालांकि वर्ष 1956 में समान नागरिक संहिता की मांग पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने समर्थकों और महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर की थी, लेकिन फिर भी कमी यह रही, कि मुस्लिम विपक्षी सदस्यों ने इसका विधिवत विरोध किया। यह भारत के औपनिवेशिक काल की बात है, जब भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था, तब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने महिलाओं को सती की बुरी प्रथा से बचाने की कोशिश की और इसके खिलाफ नियामक क़ानून पारित किया। और यही समय था जब समान नागरिक संहिता की स्थापना हुई थी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
अभी तक की बातों से यह प्रतीत होता है कि संविधान एक स्पष्ट और पारदर्शी कानूनी रूप से संहिताबद्ध प्रावधान देता है, कि पूरे क्षेत्र में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और केंद्र सरकार को हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय अर्थात् शाहबानो मामले के फैसले में यह भी निराशा की बात है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 को एक मृत पत्र बना दिया गया है। राष्ट्र के लिए एक विशिष्ट सामान्य कोड को लेकर किसी भी आधिकारिक आंदोलन का कोई सबूत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वास ने प्रगति तो की है, कि मुस्लिम लोगों के समूह को अपने स्वयं के कानून में बदलाव के मामले में नेतृत्व करना होगा। एक विशिष्ट नागरिक संहिता, परस्पर विरोधी विश्वास प्रणालियों वाले कानूनों के प्रति विभिन्न निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय समन्वय के उद्देश्य में मदद करेगी। कोई भी जन समूह इस मुद्दे पर अनावश्यक रियायतें देकर संभवत: अपना पक्ष नहीं रखने वाला है। सभी के लिए न्याय, हर मामले में समानता की तुलना में न्याय प्रदान करने का एक स्पष्ट रूप से अधिक स्वीकार्य तरीका है।
किशोर न्याय अधिनियम अर्थात् बच्चों की देखभाल और संरक्षण का निर्णय पारित करना हर तरह से समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने का एक प्रयास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार यौन अभिविन्यास असमानता को दूर करने और व्यक्तिगत कानूनों की प्रणाली के तहत अपनाई जाने वाली प्रतिगामी प्रथाओं को रद्द करने के लिए एक समान नागरिक संहिता की संरचना करे।
जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक आपराधिक संहिता है जो देश में धर्म, स्थिति, कबीले और निवास की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक है, हालांकि अलगाव और प्रगति से संबंधित कोई तुलनीय कोड नहीं है जो व्यक्तिगत कानूनों द्वारा प्रशासित होते हैं।
अगर हम बात करे गोवा की तो, स्वतंत्रता के बाद, गोवा राज्य ने पुर्तगाली नागरिक संहिता को अपनाया है जिसने अपने प्रत्येक निवासी के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया है। इस संहिता के तहत, विवाहित जोड़ा प्रत्येक साथी द्वारा दावा किए गए और प्राप्त किए गए सभी लाभों पर संयुक्त स्वामित्व रखता है। वास्तव में, माता-पिता भी अपने बच्चों को पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर संपत्ति का आधा हिस्सा उन्हें दिया जाना चाहिए। जिन मुस्लिम लोगों ने गोवा में अपनी शादी को सूचीबद्ध किया है, उन्हें बहुविवाह की अनुमति नहीं है। अर्थात् गोवा में, प्रत्येक व्यक्ति विवाह, उत्तराधिकार और तलाक से संबंधित समान कानूनों से बंधा हुआ है, न की व्यक्तिगत कानूनों के अधीन हैं।
जबकि भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 25 में कहा गया है, कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के समान रूप से हकदार हैं जो यूसीसी स्थापित होने पर समान नागरिक संहिता के विपरीत प्रावधान बन रहा है। इसलिए समान नागरिक संहिता और व्यक्तिगत कानूनों को किसी भी प्रकार के भेदभाव या असहमति के बिना संचालित होने के लिए एक संयुक्त मंच दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक संहिता केवल कानूनों का एक आधुनिक सेट है जिसे व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर शामिल किया जाना है और हमारे देश के नागरिकों द्वारा विधिवत व नए रूप से पालन किया जाना है लेकिन मुख्य प्रश्न यह है, कि क्या हो रहा है। क्या सभी मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के प्राचीन रीति-रिवाजों का नागरिकों द्वारा विधिवत पालन किया गया है। नागरिक संहिता का उचित प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन होना चाहिए अन्यथा यह हमारे देश के नागरिकों के बीच विभिन्न असहमति और भेदभाव पैदा कर सकता है क्योंकि यह नए कानूनों बनाम सभी मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों का सवाल है जिनका दशकों से पालन किया जा रहा है।
समान नागरिक संहिता! क्यों?
संविधान में वर्णित,देश के सभी निवासियों को उनके धर्म, वर्ग, स्थिति, लिंग आदि से स्वतंत्र समान दर्जा देना राज्य का कर्तव्य है। जिसके आलोक में कुछ बिंदुओं को रखना चाहेंगे……
1.यौन अभिविन्यास निष्पक्षता को आगे बढ़ाने के लिए। नागरिक संहिता दो लोगों को मानक पर लाएगा।
2.यह वोट बैंक की राजनीति को कम करेगा जो कि अधिकांश राजनीतिक दल हर चुनाव के दौरान करते हैं।
3.आधिकारिक अदालत की निगाह में सभी निवासी भारतीय समान हैं। अर्थात् व्यक्तिगत कानूनों को छोड़कर आपराधिक कानून और अन्य सामान्य कानून सभी के लिए समान हैं। इन पंक्तियों के साथ, नागरिक संहिता राष्ट्रीय जुड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
4.यह भारत को एकीकृत करेगा, भारत कई धर्मों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं वाला देश है, यह आजादी के बाद से पहले से कहीं अधिक भारत को एकीकृत करेगा। यह प्रत्येक भारतीय को उसकी जाति, धर्म या जनजाति के बावजूद एक राष्ट्रीय नागरिक संहिता के तहत लाएगा।
5.आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का संकेत, यह इस बात का संकेत है कि राष्ट्र जाति और धार्मिक राजनीति से दूर चला गया है। जबकि हमारी आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण रही है लेकिन हमारी सामाजिक वृद्धि पिछड़ गई है। एक यूसीसी समाज को आगे बढ़ने और भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा।
6.यह वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, यूसीसी का मतलब यह नहीं है कि यह लोगों की अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, इसका मतलब सिर्फ यह है कि प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और सभी को किसी भी धर्म की परवाह किए बिना समान कानूनों का पालन करना होगा।
7.परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अल्पसंख्यक लोगों को उन कानूनों को चुनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनके तहत वे प्रशासित होना चाहते हैं। ये धार्मिक कानून एक विशिष्ट अस्थायी संदर्भ में तैयार किए गए थे और बदले हुए समय में भी स्थिर नहीं रहना चाहिए।
8.पर्सनल लॉ वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली की तरह हैं जो आज भी हजारों साल पुराने मूल्यों पर चलते हैं। एक यूसीसी पूरे देश को एकीकृत करके इसे बदल देगा।
समान नागरिक संहिता! क्यों नहीं?
1.भारत में विभिन्न प्रकार की विविधता के कारण नियमों की एक विशिष्ट और समान व्यवस्था बनाना कठिन है। लेकिन हमारी सरकार नियमित सिद्धांतों पर विचार करने का प्रयास कर रही है।
2.कई लोगों के समूह, अधिकांशतः अल्पसंख्यक नेटवर्क, समान नागरिक संहिता को सख्त अवसर के लिए उनके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
3.संविधान धर्म के अवसर पर किसी के पसंदीदा विशेषाधिकार को समायोजित करता है। जो भी हो, समान दिशा-निर्देशों के संहिताकरण और इसके आवेग से धर्म के अवसर की सीमा कम हो सकती है। फलस्वरूप घरेलू मामलों में व राज्य में बाधा उत्पन होगी।
4.नागरिक संहिता लाना एक नाजुक और गंभीर काम है।
5.नागरिक संहिता के बारे में गलत सूचना, और संहिता की सामग्री को स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया जाना, जिसके आलोक में अल्पसंख्यकों का मानना है कि यह उन पर बहुमत के विचार थोपने का एक तरीका है।
6.नागरिक संहिता की जटिल और संवेदनशील प्रकृति के कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
7. विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं जो यूसीसी बहस का राजनीतिकरण करते हैं।
नागरिक संहिता से जुड़े मामले
- मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम , इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सभी भेदभावों को दूर करने में मदद करेगी और कानून के प्रति निष्ठा का भाव व्याप्त होगा।
- जॉन वल्लामट्टम और अन्य बनाम भारत संघ, इस मामले में यह विधिवत कहा गया था, कि एक सामान्य नागरिक संहिता विश्वास प्रणालियों पर निर्भर विसंगतियों को दूर करके राष्ट्रीय समावेशन के कारण में मदद करेगी।
3. सरला मुद्गल मामला,
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को खत्म किए बिना इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो सकता है और किसी अन्य महिला से शादी नहीं कर सकता है।
भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के विभिन्न धार्मिक कानूनों का एक अनूठा मिश्रण है। सभी भारतीयों के लिए एक ही क़ानून में कोई समान परिवार संबंधी कानून मौजूद नहीं है, जो भारत में सह-अस्तित्व में रहने वाले सभी धार्मिक समुदायों को स्वीकार किया जाता है। हालांकि उनमें से अधिकांश का मानना है कि यूसीसी निश्चित रूप से वांछनीय है और यह भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत और समेकित करने में काफी मददगार साबित होगा।
संपूर्ण आयामों को जानने के बाद निष्कर्षतः हम यह कह सकते है कि सामान्य नागरिक संहिता धर्म से स्वतंत्र सभी निवासियों के व्यक्तिगत मुद्दों की निगरानी के लिए बहुत सारे कानून स्थापित करेगी, सच कहा जाए तो यह वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद है। इस तरह के गतिशील परिवर्तन से न केवल सख्त आधार पर महिलाओं पर उत्पीड़न को समाप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश की मुख्यधारा की संरचना भी मजबूत होगी और एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। हमारे सामाजिक ढांचे को बदलने की जरूरत है, जो असमानताओं, अलगावों और विभिन्न चीजों से भरा हुआ है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं।
बदलते समय के साथ, धर्म से स्वतंत्र सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता उभरी है, जो यह गारंटी दे, कि उनके महत्वपूर्ण और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। दरअसल, समान नागरिक संहिता को लाकर धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को भी मजबूत किया जा सकता है।
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है जिसका अर्थ है कि किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है इसलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया है।
संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 भारत का सबसे संदिग्ध और विवादास्पद संशोधन है। दरसल हुआ ये कि भारत की प्रस्तावना, जो पहले “संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य” थी, को “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य” में बदल दिया गया।
यह इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था और इसे सबसे विवादास्पद संशोधन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लाया गया था।
यह आपातकालीन युग व्यापक रूप से अलोकप्रिय था और 42वां संशोधन सबसे विवादास्पद मुद्दा था।
जबकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरा कार्य आपातकाल के दौरान बहुमत के बिना किया गया था।
नागरिक संहिता के आने के बाद अब धर्मनिरपेक्षता को चुनौती तो मिल गई है लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उसी धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की कोई कानूनी वैधता थी या नहीं?
भारत को धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि भारत पहले से ही समुदायों को विभिन्न जातियों में विभाजित करता है और जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण प्रदान करता है और भारत प्रत्येक समुदाय को व्यक्तिगत कानून प्रदान करने के लिए इच्छुक भी है।
व्यक्तियों के अधिकारों की समान सुरक्षा नहीं है, इससे धर्मनिरपेक्षता कैसे स्थापित हो सकती है?
हमारा देश जिस तथाकथित “धर्मनिरपेक्षता” की बात करता है, उसका अपवाद समान नागरिक संहिता कैसे हो सकती है?
सभी मनुष्यों की दो आंखें, दो कान, दो नाक हैं, हर कोई भारत की एक ही मिट्टी से जुड़ा है और वे एक ही हवा में सांस लेते हैं, यहां तक कि संविधान भी उन्हें एक ही स्तर पर रखता है, फिर कानूनों में कोई विसंगति क्यों होनी चाहिए।
कानून सभी के लिए समान होने चाहिए, एक राष्ट्र होने के कारण एक नियम होना चाहिए।
धन्यवाद!
ये एपिसोड हमारे व्यूवर को कैसा लगा हमे कमेंट करके बताए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए।जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाए।जँहा हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबध्य रूप में प्रस्तुत कर दिया है।